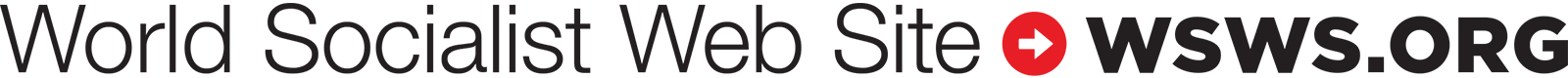यह हिंदी अनुवाद अंग्रेजी के मूल All We Imagine as Light director Payal Kapadia speaks with WSWS जो 31 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुआ थाI
पिछले महीने राइटर/डायरेक्टर पायल कपाड़िया (39) ने अपनी पहली फ़िक्शन फ़िल्म 'ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट' को लेकर डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस से बात की। यह फ़िल्म 2024 में आयोजित 77वें कांस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता था।
'ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट', मज़दूर वर्गीय पृष्ठभूमि की उन तीन महिलाओं का बहुत गहरा मानवीय चित्रण है जो उस शहर में जीने का संघर्ष कर रही हैं। यह फ़िल्म केरल से आने वाली प्रवासी वर्कर प्रभा और अनु और कैंटीन में काम करने वाली, रत्नागिरि की पार्वती पर केंद्रित है और इस बड़े शहर में उनका साझा संघर्ष ही उनके बीच एक रिश्ते का आधार बनता है। इस फ़िल्म को प्रसारित करने के लिए अभी तक पचास से अधिक देशों में डिस्ट्रिब्यूशन डील हो चुकी हैं और अमेरिका में कई स्ट्रीमिंग सेवाओं पर यह उपलब्ध है।
रिचर्ड फिलिप्सः हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया और 'ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट' इसके क़िरदारों को बधाई। आपने अपनी फ़िल्म के सेट के लिए मुंबई को क्यों चुना और तीन स्वास्थ्य कर्मियों पर ही कहानी कहना क्यों चुना, जिनकी समकालीन सिनेमा में कोई पूछ नहीं होती है?
पायल कपाड़ियाः बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, इसे मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था क्योंकि सूरत में उसका व्यापारिक अधिकार ख़त्म हो गया था और उसे एक नया बंदरगाह बनाना था। उससे पहले यह द्वीपों पर बसे छोटे छोटे कई गांवों का समूह हुआ करता था। यह इलाक़ा किंग चार्ल्स द्वितीय की पत्नी कैथरीन के दहेज का हिस्सा था, जो पुर्तगाल के राजा की बेटी थी। अंग्रेज़ी राजा को उस समय लगा था कि यह ज़मीन ब्राज़ील में है।
इस शहर की बुनियाद मुख्य रूप से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के अतीत से जुड़ी हुई थी और यह एक ऐसा शहर है जिसे मैं और जानना समझना चाहती थी। यह शहर उन लोगों के हाथों बना है जो यहां के नहीं थे और उन्हें पूरे देश से यहां रहने और काम करने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने इसे विकसित किया। बीते 20 से 30 सालों में उस इतिहास को नकारने या उसे मिटाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यह ऐसा शहर है जिसका वजूद इन लोगों के यहां आकर रहने और काम करने से पहले था ही नहीं।
रिचर्ड फिलिप्सः और कहानी क्यों तीन स्वास्थ्य कर्मियों पर केंद्रित है?
पायल कपाड़ियाः इसके निजी कारण हैं, जब मैंने फ़िल्में लिखनी शुरू की तो मैंने अस्पतालों में और वेटिंग रूम्स में काफ़ी समय बिताया। आपको बहुत आसानी से दिख जाता है कि अस्पताल कैसे काम करते हैं और ये भी कि नर्सें ही इन जगहों को मुख्य रूप से चलाती हैं। डॉक्टर बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ मिनटों के लिए और फिर ग़ायब हो जाते हैं।
जिन लोगों से मैं मिल रही थी, उनमें अधिकांश नर्सें थीं और इसीलिए मैं चाहती थी कि उन महिलाओं पर एक फ़िल्म बनाऊं जो काम के लिए मुंबई आई थीं। भारत में एक महिला के लिए नर्सिंग को अपने गृह राज्य छोड़कर मुंबई जैसे शहरों में जाने का एक जायज पेशा माना जाता है।
नर्सों ने मेरे लिए बहुस्तरीय क़िरदारों को रच ने और उनकी बाहरी और भीतरी ज़िंदगी में झांकने की संभावना पैदा की। इस पेशे को अपनाने वाली महिलाओं के लिए विरोधाभास और भी तीखे हैं।
जैसा कि एक क़िरदार कहती है, 'अगर आप नर्स हैं तो आप अपनी भावनाएं ज़ाहिर नहीं कर सकतीं।' मुख्य क़िरदार प्रभा, किसी तरह के भावनात्मक होने से बचने के लिए इसे एक कवच की तरह इस्तेमाल करती है।
नर्सिंग कोई बहुत बढ़िया पेशा नहीं है- आपको शरीर से निकलने वाले बहुत सारे द्रवों, जैसे मवाद, खून और ऐसी ही बहुत सी चीजों से निपटना होता है- लेकिन इस फ़िल्म ने और बहुत सी चीजों के बारे में बात करने का मुझे मौका दिया।
भारतीय सिनेमा में नर्सिंग को दिखाना थोड़ी जटिलता वाला रहा है। अगर आपने सत्यजीत रे की 'प्रतिद्वंद्वी' (1970) देखी है, जोकि उनकी कोलकाता ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या आशय है। उस फ़िल्म में नर्स को एक कमज़ोर महिला के रूप में दिखाया गया है क्योंकि वह अकेली रहती है और नौकरी करती है।
रिचर्ड फिलिप्सः आपकी फ़िल्म कई स्तरों और उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में बात करती है। क्या इस फ़िल्म के बनने और इसके क़िरदारों को गढ़ने की प्रक्रिया में अभिनेत्रियों का सीधा जुड़ाव था?
पायल कपाड़ियाः जब डॉयलॉग लिखे जा रहे थे, अभिनेत्रियों ने मेरी बहुत मदद की। वे सभी बहुत ऊंचे दर्ज़े की अभिनेत्रियां हैं और अपने क़िरदार में उन्होंने बहुत डूब कर काम किया और बहुत सी बारीक़ चीज़ों को सामने ले आईं।
पार्वती का क़िरदार निभाने वाली छाया कदम अस्पताल में खाना बनाती हैं और रत्नागिरि की रहने वाली हैं, जो मुंबई के दक्षिण में है। पार्वती की तरह ही उनका भी परिवार मुंबई चला आया था। उनके पिता एक कॉटन मिल में काम करते थे, जैसे पार्वती के पति काम करते हैं। रत्नागिरी से मुंबई आने के इतिहास और खदान मालिकों की बर्ख़ास्तगी और 1982 में हड़ताल के बाद अपने घरों से महरूम हो चुके वर्करों की दास्तान से वह अच्छी तरह वाक़िफ़ थीं। (इस हड़ताल को ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, जिसमें ढाई लाख मिल वर्करों ने हिस्सा लिया था।)
जिस तरह से उनका पलायन हुआ था, उस नज़रिए से भी उन्होंने अपने क़िरदार में काफ़ी बारीकियां डालीं और अपने डॉयलॉग में कुछ ऐसे शब्द जोड़े जो स्वाभाविक रूप से अनुवाद के दौरान खो गए। अपने क़िरदार को होने वाली मुश्किलों को एक ख़ास तरह का हल्कापन देने का उनमें शानदार हुनर था और एक ऐसा रवैया था जो मुंबई की ज़िंदगी में रचा बसा हो।
रिचर्ड फ़िलिप्सः मिलों में काम करने के लिए दक्षिण भारत से कितने लोग आए होंगे?
पायल कपाड़ियाः यह पलायन ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी में और पूरे 20वीं सदी में हुआ था। आज़ादी के बाद, मिलें उन लोगों के हाथों में चली गईं जो पहले अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। रत्नागिरि से बहुत सारे लोग आए थे, जोकि फ़िल्म में भी है। मुंबई की पहचान, खान पान की प्रकृति, भाषा, बोली और जिस तरह वे हिंदी बोलते हैं, इस पर कोंकण इलाक़ा, दक्षिण मुंबई और जहां रत्नागिरि है, उसका बहुत प्रभाव है।
रिचर्ड फिलिप्सः फ़िल्म में एक डबिंग में कहा जाता है, 'मुंबई भ्रमों का शहर है और इसमें अनकहा नियम है कि अगर आप गटर में भी हैं तो आपको गुस्सा होने का हक़ नहीं है।' क्या इस पर आप प्रकाश डाल सकती हैं?
पायल कपाड़ियाः हां, मुंबई के लोग, जिन्हें मुंबईकर कहा जाता है, उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि जब भी कोई भयानक घटना घटती है जैसे बाढ़, तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें बताया गया कि यही “मुंबई की स्पिरिट“ (जीजीविषा) है और आधिकारिक बहसों में इसका बहुत अधिक ज़िक्र किया जाता है।
लोग उन हालात में एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। राज्य रोज़ाना स्तर पर लोगों के लिए किसी तरह की व्यवस्था मुहैया नहीं कराता।
चाहे वह आवास के अधिकार का मामला हो या पानी या बिजली हो, ये सारी चीजें इतनी जर्जर हालत में हैं कि लोगों के पास एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इसी को “स्पिरिट ऑफ़ मुंबई“ के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन मेरे लिए और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए भी, यह ज़रूरी है कि इसे आलोचनात्मक नज़रिए से देखा जाना चाहिए।
हमारे जैसे देशों में शहरी जगहें ही ऐसी जगहें हैं जो काम देती हैं। शहर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग यहां रहने और काम करने के लिए आते हैं उनके लिए अभी भी आधारभूत ढांचा नहीं मुहैया नहीं कराया जाता है। शहरों में इस तरह की संभावनाओं का यूटोपिया (स्वप्नलोक) होता है, जोकि असलियत में होता ही नहीं।
जब हम रत्नागिरि में शूट करने गए, जिसका मुंबई पलायन करने का एक लंबा इतिहास रहा है, वहां आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था, जैसे अस्पताल, सड़कें आदि। लोगों को मुंबई जाना पड़ता था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह बहुत जटिल है लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे लेकर मैंने बहुत हताशा महसूस की और इस हताशा को फ़िल्म के ज़रिये ज़ाहिर करना चाहती थी।
रिचर्ड फिलिप्सः अभी लॉस एंजिलिस में जंगल की आग लगी थी, जोकि भ्रमों का एक और शहर है और वहां आधारभूत ढांचों की कोई कमी नहीं थी। जब भी ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगती है या बाढ़ आती है तो लोगों को बताया जता है कि कितनी शानदार बात है कि लोग एकजुट हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसे “ओज़ि स्पिरिट“ कहा जाता है, लेकिन यह सरकार के नकारेपन को महज औचित्य ठहराना होता है।
पायल कपाड़ियाः हां, बिल्कुल भारत की तरह।
रिचर्ड फिलिप्सः क्या आप अनु और शियाज़ के लव अफ़ेयर के बारे में कुछ कह सकती हैं और पश्चिमी पाठकों के लिए, क्या आप मुस्लिम विरोधी हिस्टीरिया और “लव जिहाद“ की कांस्पिरेसी थ्योरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
पायल कपाड़ियाः भारत में इसके बारे में कई सारी फ़िल्में हैं, ख़ासकर फ़िक्शन फ़िल्में, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है।
भारत में विवाह किसी की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और यह वाक़ई जाति और धर्म को देखकर किया जाता है। यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है जब आप अपनी जाति या धर्म से बाहर किसी से शादी करते हैं और ख़ासकर तब जब भारत में अभी बहुत मजबूत इस्लामोफ़ोबिक कालखंड चल रहा हो।
हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के बीच विवाह या प्यार को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो वे ऐसा क़ानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह के विवाहों के लिए मुस्लिम पुरुषों को अपराधी घोषित करता है।
यह उन युवा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो वाक़ई प्यार में हैं और उनके माता पिता इस पर सहमत नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है और जब जोड़े साथ भागते हैं तो वे इसे लव जिहाद का नाम देते हैं।
इस हालात से निपटना युवा जोड़े के लिए ख़ासकर बहुत मुश्किल साबित होता है, इसीलिए यह बहुत अहम है कि मेरी फ़िल्म में उन्हें उनकी पहचान तक सीमित नहीं किया गया है, जोकि आधिकारिक राजनीतिक बहसों में हो रहा है।
मैं जोड़े को इतना शानदार और प्यारा दिखाना चाहती थी कि कोई भी खुद को इससे जोड़कर देख सके। अगर आप भारतीय हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका रिश्ता आपके दिल में भी एक डर पैदा करता है कि उनके लिए यह कितना मुश्किल होने जा रहा है।
रिचर्ड फिलिप्सः फ़िल्म के सभी क़िरदार अलग अलग किस्म की मौजूदा रूढ़ियों (टैबू) से जूझ रहे हैं। सभी तीनों महिलाएं आर्थिक समस्याओं और अन्य दबावों का सामना कर रही हैं और हालांकि आप इसे सीधे संबोधित नहीं करतीं लेकिन टैबू को कमज़ोर करती हैं। वे मोबाइल फ़ोन, आधुनिक संचार और अन्य बदलावों वाली दुनिया में रहती हैं। फ़िल्म का अंतिम हिस्सा उम्मीदों से भरा है। क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
पायल कपाड़ियाः इन महिलाओं के बीच दोस्ती का यह एक किस्म का यूटोपियाई क्षण है। उनके बीच एक समझ है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहते हुए, हालांकि हरेक को अपनी निजी ज़िंदगी में एक लंबी यात्रा करनी है, उन्हें एक दूसरे के साथ सुकून और आराम मिलता है।
जब भारत में लोगों के एक साथ आने की बात आती है और अन्य जगह भी, तो अक्सर उस एकता की राह में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और पहचान आड़े आ जाती है। उनके बीच के मेलजोल के छोटे पल में मैं इस कमी को भरना चाहती थी और कहना चाहती थी कि अगर वे एक ही भाषा नहीं बोलती हैं या एक जाति और धर्म की नहीं है तब भी, दोस्ती और लगाव एक दूसरे को सहारा देने के तरीक़े हो सकते हैं।
रिचर्ड फिलिप्सः और यह वर्ग का भी सवाल है। उनके बीच समान वर्गीय हित भी हैं।
पायल कपाड़ियाः यह सही है।
रिचर्ड फिलिप्सः इस फ़िल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और समीक्षकों की खूब सराहना मिली, भारत में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या इसकी उन ज़िलों में स्क्रीनिंग हुई जहां इसे फ़िल्माया गया था या उन स्वास्थ्य कर्मियों को ये फ़िल्म दिखाई गई?
पायल कपाड़ियाः हमने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बहुत सारी स्क्रीनिंग की है, ख़ासकर केरल में, जोकि फ़िल्म की भाषा भी है। हमने सिर्फ़ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कामकाजी महिलाओं के बीच भी स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया है।
फ़िल्म को स्ट्रीमिंग वेबसाइटों पर भी रिलीज़ किया गया है, जहां हर कोई इसे देख सकता है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास इनके सब्सक्रिप्शन होते हैं क्योंकि वहां क्रिकेट का भी प्रसारण होता है। जो लोग अभी सिनेमा हाल में नहीं जा सकते वे अपने मोबाइल उपकरणों पर अलग अलग भाषाओं में सबटाइटिल में इसे देख सकते हैं, इसलिए यह पूरे देश में उपलब्ध है।
हमने कई अलग अलग शहरों में बहुत सारी महिलाओं के बीच इसकी फ़्री स्क्रीनिंग की है, जोकि बहुत सीखने वाली बात रही क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे डांट भी लगाई। मुझे लगता है कि अपने दर्शकों से सीखना एक फ़िल्म मेकर के लिए बहुत ही अहम बात है। ये दर्शक अलग अलग चीजों की ओर इशारा करेंगे या ऐसी बातें सुझाएंगे जिसे एक ख़ास दिशा में दिखाया जा सकता था। पार्वती के और बहुत सारे पहलू हैं जो फ़िल्म में शामिल नहीं किए गए, और जिसे किया जा सकता था, और मुझे कुछ अफसोस भी है।
रिचर्ड फिलिप्सः आपकी फ़िल्म ने कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिनमें पिछले साल कान्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल भी शामिल है, लेकिन आगामी ऑस्कर के लिए विदेशी भाषा की श्रेणी में भेजने के लिए भाीरतीय फ़िल्म प्रशासन ने इसे नहीं चुना।
फ़िल्म फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष ने कथित रूप से कहा था कि 'सेलेक्शन कमेटी को लगा कि वे एक ऐसी यूरोपीय फ़िल्म देख रहे हैं जिसे भारत में बनाया गया था, ऐसी भारतीय फ़िल्म नहीं जिसे भारत में बनाया गया हो।' आपकी कोई टिप्पणी?
पायल कपाड़ियाः किसी को यह बताना पड़ेगा कि भारतीय क्या है, क्योंकि उनका जो आशय है उससे मैं कन्फ़्यूज़ हूं। मैं भारतीय हूं, और हां, यह एक भारतीय फ़िल्म है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे इससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
रिचर्ड फिलिप्सः सत्यजीत रे ने एक बार कहा था कि 'महान सिनेमा वह है जिसमें क्षेत्रीय बंधनों को छोड़कर एक सार्वभौमिक स्तर तक उठने की क्षमता होती है।' निश्चित रूप से 'ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट' ऐसा करती है।
पायल कपाड़ियाः मुझे यह भी लगता है कि भारत में सिनेमा की भाषा के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, जोकि हमारे उप महाद्वीप के लिए बहुत विशिष्ट है। पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र को हमारे सौंदर्यशास्त्र के साथ समग्र सिनेमाई विमर्श के हिस्से के रूप में देखने की ज़रूरत है। भारतीय फ़िल्मों में अभिनय, गाने, ये सभी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सिनेमा में बहुलता और विविधता मौजूद हो।
रिचर्ड फिलिप्सः एक अंतिम सवाल, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है?
पायल कपाड़ियाः अगला प्रोजेक्ट, यह हमेशा ही एक जटिल सवाल है। पिछले चार या पांच सालों में मैंने दो फ़िल्मों पर एक साथ काम किया- 'ए नाइट ऑफ़ नोईंग नथिंग' और 'ऑल वी इमेजिन ऐज़ लाइट'- और अभी दो अन्य स्क्रिप्टों पर काम करना शुरू किया है। इनकी भी पृष्ठभूमि मुंबई ही है, इसलिए मैं यह देखने की कोशिश कर रही हूं कि क्या इस शहर में रहने और काम करने वाले लोगों पर यह कोई ट्रायोलॉजी हो सकती है।
मैं बहुत रिसर्च करती हूं, जिसमें समय लगता है और यह लगभग डाक्युमेंट्री जैसी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें लोगों से मिलना पड़ता है और बहुत सारे इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। मैं इस प्रक्रिया का आनंद लेती हूं और इसे बहुत सही प्रक्रिया मानती हूं और इससे बहुत कुछ सीखती हूं।